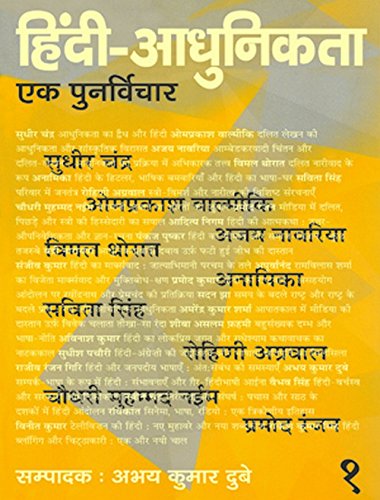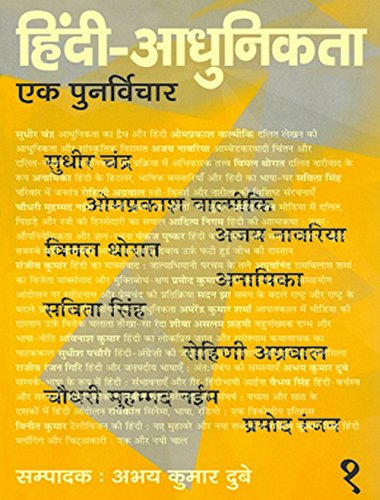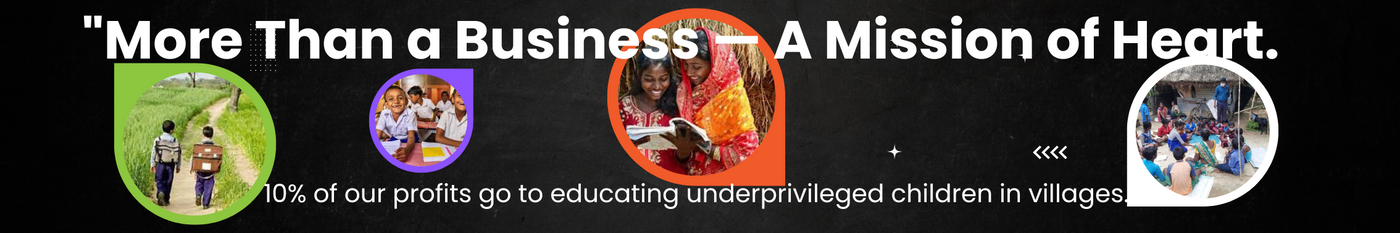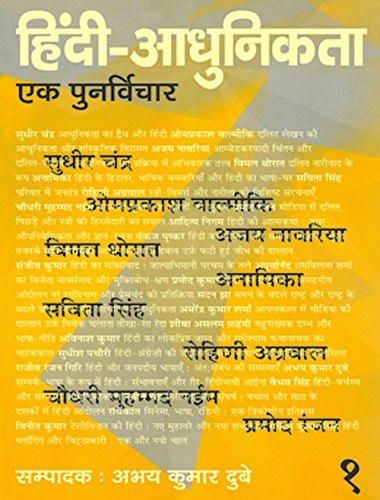Hindi Adhunikta Ek Punarvichar (I,II,III VOL) (3 vol)
Hindi Adhunikta Ek Punarvichar (I,II,III VOL) (3 vol) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Genuine Products Guarantee
Genuine Products Guarantee
We guarantee 100% genuine products, and if proven otherwise, we will compensate you with 10 times the product's cost.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Products are generally ready for dispatch within 1 day and typically reach you in 3 to 5 days.
Author: Abhay Kumar Dubey
Brand: Vani Prakashan Publisher
Binding: hardcover
Details: Hindi-Aadhunikta : Ek Punarvichar (3 Vol. Set)
EAN: 9789350726228
Package Dimensions: 9.1 x 6.6 x 1.1 inches
Languages: Hindi
हिन्दी-आधुनिकता - 1,2,3
हिन्दी भाषा का सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विन्यास पिछले पचास सालों में काफ़ी कुछ बदला है। आज की हिन्दी विविध उद्देश्यों को पूरा कर सकने वाली और समाज के विविध तबकों की बौद्धिक व रचनात्मक आवश्यकताएँ व्यक्त कर सकने वाली एक ऐसी सम्भावनाशील भाषा है जो अपनी प्रचुर आन्तरिक बहुलता और विभिन्न प्रभाव जज़्ब करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। देशी जड़ों वाली एक मात्र अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की ग्राहकता में उल्लेखनीय उछाल आया है, और वह अंग्रेज़ी की तत्सम्बन्धित दावेदारियों को गम्भीर चुनौती देने की स्थिति में है। ज़ाहिर है कि हिन्दी वह नहीं रह गयी है जो वह थी मात्रात्मक और गुणात्मक तब्दीलियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। इन्हीं सब कारणों से हिन्दी की प्रचलित जीवनी पर पड़ी तारीख़ बहुत पुरानी लगने लगी है। यह भाषा अपने नए जीवनीकारों की तलाश कर रही है।
२३ सितम्बर से २९ सितम्बर, २००९ के बीच शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में हुए वर्कशॉप में हिन्दी से सम्बन्धित उन प्रश्नों पर दुबारा ग़ौर किया गया जिन्हें आज से चालीस-पैंतालीस साल पहले अन्तिम रूप से तय मान लिया गया था। सत्ताईस विद्वानों के बीच सात दिन तक अहर्निश चले बहस-मुबाहिसे के एक-एक शब्द को टेप किया गया। करीब एक हज़ार पृष्ठों में फैले इस टेक्स्ट को सम्पादित करने की स्वाभाविक दिक्कतों के बावजूद पूरी कोशिश की गयी कि मुद्रित पाठ को हर तरह से पठनीय बना कर, दोहराव और अस्पष्टताएँ निकाल कर उनके मानीखेज कथनों को उभारा जाये। वर्कशॉप की बहस को इस शैली में प्रस्तुत करने का यह उदाहरण हिन्दी के लिए सम्भवतः पूरी तरह से नया है।
इस अध्ययन सप्ताह की शुरुआत इतिहासकार सुधीर चन्द्र द्वारा दिये गये बीज-वक्तव्य से हुई। दलित-विमर्श और स्त्री विमर्श हिन्दी की अपेक्षाकृत दो नयी धाराएँ हैं जिन्होंने इस भाषा की आधुनिकता के स्थापित रूपों को प्रश्नांकित करने की भूमिका निभायी है। दलितों और स्त्रियों द्वारा पैदा की गयी बेचैनियों को स्वर देने का काम ओमप्रकाश वाल्मीकि, अजय नावरिया, विमल थोराट, अनामिका, सविता सिंह और रोहिणी अग्रवाल ने किया। स्त्री-विमर्श में आनुषंगिक भूमिका निभाते हुए उर्दू साहित्य के विद्वान चौधरी मुहम्मद नईम ने यह सवाल पूछा कि क्या स्त्रियों की ज़ुबान मर्दों के मुक़ाबले अधिक मुहावरेदार होती है।
वर्कशॉप में हिन्दी को ज्ञान की भाषा बनाने के उद्यम से जुड़ी समस्याओं और ऐतिहासिक उलझनों की पड़ताल आदित्य निगम और पंकज पुष्कर ने की। बद्री नारायण ने हिन्दी साहित्य के भीतर आधुनिकतावादी और देशज प्रभावों के बीच चल रही जद्दोजहद का खुलासा किया। दूसरी तरफ राजीव रंजन गिरि ने हिन्दी और जनपदीय भाषाओं के समस्याग्रस्त रिश्तों को कुरेदा। तीसरी तरफ़ सुधीश पचौरी ने हिन्दी पर पड़ रहे अंग्रेज़ी के प्रभाव की क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त की रोशनी में विशद व्याख्या की। नवीन चन्र्त ने साठ के दशक में चले अंग्रेज़ी विरोधी आन्दोलन की पेचीदगियों का आख्यान प्रस्तुत किया। अभय कुमार दुबे ने हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने के सन्दर्भ में ग़ैर-हिन्दीभाषियों के हिन्दी सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण पेश किया। वैभव सिंह ने सरकारी हिन्दी बनाने की परियोजना के विफल परिणामों को रेखांकित किया। अमरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि आपातकाल के राजनीतिक संकट ने हिन्दी के साहित्यिक और पत्रकारीय बुद्धिजीवियों की लोकतन्त्र के प्रति निष्ठाओं को किस तरह संकटग्रस्त किया था।
स्त्री और दलित विमर्श के उभार से पहले हिन्दी की दुनिया राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी विमर्श से निर्देशित होती रही है। इन दोनों विमर्शो की प्रभुत्वशाली भूमिका की आन्तरिक जाँच-पड़ताल का काम सदन झा, प्रमोद कुमार, अपूर्वानन्द और संजीव कुमार ने किया। शीबा असलम फ़हमी की प्रस्तुति में हिन्दी और बहुसंख्यकवादी विमर्श के बीच सम्बन्धों की संरचनात्मक प्रकृति का उद्घाटन किया गया। अविनाश कुमार ने राधेश्याम कथावाचक पर किए गए अनुसन्धान के ज़रिये दिखाया कि साहित्य के रूप में परिभाषित होने वाली सामग्री कैसे वाचिक और लोकप्रिय के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाती है। रविकान्त ने सिनेमा और भाषा के बीच सम्बन्धों के इतिहास को उकेरा, प्रमोद कुमार ने मीडिया में हाशियाग्रस्त समुदायों की भागीदारी का प्रश्न उठाया, राकेश कुमार सिंह ने चिट्ठाकारी (ब्लॉगिंग) के हिन्दी सम्बन्धी अध्याय की जानकारी दी और विनीत कुमार ने उस विशिष्ट प्रक्रिया को रेखांकित किया जिसके तहत टीवी की हिन्दी बन रही है।